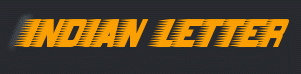हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। यह आशंका देश के दिग्गज भू वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है।
इसी वजह से जून में देहरादून में देश भर के भूवैज्ञानिक जुटे। उन्होंने वाडिया में ”अंडरस्टैंडिंग हिमालयन अर्थक्वेक्स” पर और एफआरआई देहरादून में ”अर्थक्वेक रिस्क एसेसमेंट” पर मंथन किया। इनमें वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि अब जो भी बड़ा भूकंप आएगा, उसकी तीव्रता करीब 7.0 होगी। उन्होंने बताया कि 4.0 तीव्रता के भूकंप में जितनी ऊर्जा निकलती है, उससे करीब 32 गुना अधिक ऊर्जा 5.0 तीव्रता के भूकंप से निकलती है। मौजूदा समय में जो धीमे भूकंप आ रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कहा जा सके कि भूगर्भ से सारी ऊर्जा निकल गई है। शोध में पाया गया है कि बड़े भूकंप आने के कुछ साल या कुछ महीने पहले धीमे भूकंप आने का सिलसिला बढ़ जाता है।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में प्रदेश में 22 बार 1.8 से लेकर 3.6 तीव्रता तक के भूकंप आए हैं। जिनके झटके सर्वाधिक चमोली, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और बागेश्वर में महसूस हुए हैं। उत्तराखंड संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 4 व 5 में है। यहां 1991 में उत्तरकाशी में 7.0 व चमोली में 1999 में 6.8 तीव्रता के भूकंप आए थे, तब से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। जिससे वैज्ञानिक जल्द बड़े भूकंप की आशंका जता रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ.विनीत गहलोत ने इसकी वजह उत्तराखंड में भूगर्भीय प्लेटों की गति लॉक्ड होना बताया है।
पूर्वानुमान बहुत ही मुश्किल
भूकंप के संबंध में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में दो जीपीएस लगाए गए हैंं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है।
क्यों आता है भूकंप
जब भूगर्भ में दबाव बढ़ता है तो चट्टानों में दरारें हो जाती हैं, जिससे हल्के भूकंप पैदा होते हैं, लेकिन भूगर्भ में मौजूद पानी इन दरारों को भरने लगता है, जिससे हल्के भूकंप आने का सिलसिला रुक तो जाता है, लेकिन फिर अचानक बड़ा भूकंप आता है। चमोली और उत्तरकाशी में भूकंप आने के पहले ऐसी प्रवृत्ति देखी गई थी।
मैदान या पहाड़, कहां ज्यादा नुकसान होगा
वाडिया में आयोजित कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने कहा कि मैदान हो या पहाड़, अगर दोनों ही जगह पर समान तीव्रता के भूकंप आते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में नुकसान कम, मैदानी क्षेत्र में अधिक होगा। बड़े भूकंप भूगर्भ में महज 10 किमी के आसपास की गहराई में आए हैं। यह अधिक गहराई के भूकंप से तीन गुना खतरनाक होते हैं। नेपाल में वर्ष 2015 में आया भूकंप अधिक गहराई में आया था, जिससे इसकी तीव्रता के मुताबिक नुकसान कम हुआ।
देहरादून की जमीन की मजबूती का होगा परीक्षण
हिमालय में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इस क्षेत्र के कुछ शहरों का चयन केंद्र सरकार ने अध्ययन के लिए किया है, जो सीएसआईआर बेंगलूरू करेगा। इसमें संवेदनशील होने की वजह से देहरादून को भी शामिल किया गया है। अध्ययन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाएगा कि दून की जमीन किस तरह की चट्टान से बनी है और उसकी मोटाई कितनी है। इस दिशा में पहले भी वाडिया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सिस्मिक माइक्रोजोनेशन किया है, लेकिन अब सीएसआइआर बेंगलूरू ने दून की मजबूती की दिशा में विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया है।
उत्तर-दक्षिण टेक्टोनिक तनाव के कारण हिमालय लगातार खिसक रहा है। प्लेटें आमतौर पर हर साल लगभग दो सेंटीमीटर खिसकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी गति बहुत धीमी है। दो प्लेटों की गति के बीच विसंगति से एक भाग ”लॉक्ड” हो जाता है, जो टेक्टोनिक तनाव का कारण बनता है। नेपाल में इसी तरह की स्थितियों के कारण भूकंप की घटनाएं हुई हैं। – डॉ. विनीत गहलोत, निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के लिए 169 जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं। यह सेंसर 5 तीव्रता से अधिक का भूकंप आने के 15 से 30 सेकेंड पहले चेतावनी देगा। इस बारे में लोगों को मोबाइल पर भूदेव एप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में लोग अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। -विनोद कुमार सुमन, आपदा सचिव
पूरे हिमालय क्षेत्र में ऊर्जा एकत्र है। कहीं-कहीं पर यह ऊर्जा निकल जाती है, लेकिन समय के साथ एकत्र भी होती रहती है, ऐसे में मध्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय में काफी अधिक ऊर्जा एकत्रित है, ये कब निकलेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। -डॉ इम्तियाज परवेज, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर, बेंगलूरू